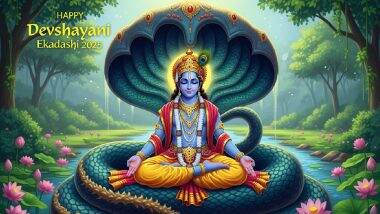
Devshayani Ekadashi 2025: हिन्दू पंचांग में कुछ तिथियां केवल तारीखें नहीं होतीं; वे एक विशाल ब्रह्मांडीय घड़ी की महत्वपूर्ण घड़ियां होती हैं, जो हमें लौकिक, दैवीय और व्यक्तिगत स्तर पर होने वाले परिवर्तनों का संकेत देती हैं. ऐसी ही एक असाधारण तिथि है देवशयनी एकादशी. यह केवल एक दिन के उपवास और पूजा का अवसर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा महत्वपूर्ण मोड़ है जहां से ब्रह्मांड की लय बदल जाती है. यह वह दिन है जब सृष्टि के पालनहार, भगवान विष्णु, चार महीनों के लिए अपनी योगनिद्रा में चले जाते हैं, और इसी के साथ चातुर्मास का पवित्र काल आरंभ होता है.
यह एकादशी अपने आप में कई दुनियाओं को समेटे हुए है. इसे देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस दिन देवता शयन करते हैं. इसे हरिशयनी या पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, जो इसका संबंध भगवान हरि (विष्णु) और पद्म पुराण जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों से जोड़ता है. महाराष्ट्र में इसे आषाढ़ी एकादशी कहते हैं, जो इसे आषाढ़ महीने की पहचान और पंढरपुर की विश्व प्रसिद्ध वारी (तीर्थयात्रा) के चरमोत्कर्ष से जोड़ती है. नामों की यह विविधता इस त्योहार की अखिल भारतीय स्वीकार्यता और विभिन्न सांस्कृतिक एवं पौराणिक परंपराओं में इसकी गहरी जड़ों को दर्शाती है. यह एक ऐसा बिंदु है जहाँ ब्रह्मांडीय घटना (देवता का शयन), स्थलीय घटना (चातुर्मास का आरंभ और पंढरपुर यात्रा का समापन) और व्यक्तिगत घटना (आंतरिक अनुशासन और साधना का समय) एक साथ मिलते हैं.
यह लेख आपको देवशयनी एकादशी 2025 की एक विस्तृत यात्रा पर ले जाएगा. हम न केवल इसके शुभ मुहूर्त और पूजा विधि को जानेंगे, बल्कि इसकी पौराणिक कथाओं, गहरे आध्यात्मिक अर्थों और इसके सबसे जीवंत मानवीय उत्सव, पंढरपुर वारी का भी अन्वेषण करेंगे. अंत में, हम यह भी देखेंगे कि इस प्राचीन आस्था का आधुनिक विज्ञान से क्या आश्चर्यजनक संबंध है.
भाग 1: दिव्य समय सारिणी: देवशयनी एकादशी 2025 का पंचांग और मुहूर्त
किसी भी व्रत या अनुष्ठान की सफलता उसके सही समय पर पालन करने में निहित होती है. देवशयनी एकादशी के लिए पंचांग का ज्ञान अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें व्रत, पूजा और पारण के लिए सबसे शुभ समय की जानकारी देता है.
1.1. तिथि और पारण: व्रत के लिए पवित्र समय-सीमा
हिन्दू धर्म में व्रत का दिन सूर्योदय के समय प्रचलित तिथि के आधार पर तय होता है, जिसे 'उदया तिथि' कहते हैं. इसी सिद्धांत के अनुसार, 2025 में देवशयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई, रविवार को रखा जाएगा, भले ही एकादशी तिथि 5 जुलाई की शाम से ही शुरू हो जाएगी.
व्रत को समाप्त करने की प्रक्रिया को 'पारण' कहा जाता है, और इसका भी एक विशिष्ट समय होता है. शास्त्रों के अनुसार, एकादशी का पारण द्वादशी तिथि के भीतर सूर्योदय के बाद ही करना चाहिए. द्वादशी तिथि समाप्त होने के बाद पारण करना पाप के समान माना जाता है. इसलिए, भक्तों को इस समय-सीमा का विशेष ध्यान रखना चाहिए.
तालिका 1: देवशयनी एकादशी 2025 - प्रमुख समय
| विवरण | तिथि और समय |
| एकादशी तिथि प्रारम्भ | 5 जुलाई 2025, शाम 06:58 बजे |
| एकादशी तिथि समाप्त | 6 जुलाई 2025, रात 09:14 बजे |
| व्रत का दिन | 6 जुलाई 2025, रविवार |
| पारण का समय | 7 जुलाई 2025, सुबह 05:29 बजे से 08:16 बजे तक |
| द्वादशी तिथि समाप्त | 7 जुलाई 2025, रात 11:10 बजे |
1.2. शुभ संयोग: शुभ मुहूर्त और चौघड़िया
वर्ष 2025 में देवशयनी एकादशी कई अत्यंत शुभ ज्योतिषीय योगों के साथ आ रही है, जो इस दिन के आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा देते हैं. इस दिन रवि योग, त्रिपुष्कर योग और साध्य योग जैसे शक्तिशाली योग बन रहे हैं.
इन योगों का एक साथ बनना यह दर्शाता है कि यह दिन आध्यात्मिक साधना के लिए ब्रह्मांडीय रूप से "सुपरचार्ज" है. रवि योग किसी भी कार्य की सफलता को बढ़ाता है और अशुभ प्रभावों को समाप्त करता है. त्रिपुष्कर योग किए गए कार्यों के फल को तीन गुना कर देता है, और साध्य योग किसी भी प्रयास में सिद्धि या पूर्णता प्रदान करता है. इन योगों की उपस्थिति का अर्थ है कि इस दिन की गई पूजा, व्रत और दान का फल कई गुना अधिक मिलता है.
इसके अतिरिक्त, दिन भर में कई अन्य शुभ मुहूर्त भी रहेंगे, जैसे ब्रह्म मुहूर्त, जो आत्म-चिंतन और ध्यान के लिए सर्वोत्तम है, और अभिजीत मुहूर्त, जो किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है.
जो लोग अपनी दिनचर्या की योजना चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार बनाते हैं, उनके लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ है. चौघड़िया दिन और रात के समय को आठ भागों में विभाजित करता है और प्रत्येक भाग की शुभता या अशुभता को दर्शाता है.
तालिका 2: 6 जुलाई 2025 के शुभ चौघड़िया मुहूर्त
| मुहूर्त का प्रकार | समय (दिन) | समय (रात) | प्रकृति |
| चर | सुबह 07:13 से 08:57 तक | रात 09:54 से 11:10 तक | सामान्य |
| लाभ | सुबह 08:57 से 10:42 तक | देर रात 01:21 से 02:38 तक (7 जुलाई) | उन्नति |
| अमृत | सुबह 10:42 से दोपहर 12:26 तक | रात 08:39 से 09:54 तक | सर्वोत्तम |
| शुभ | दोपहर 02:10 से 03:54 तक | रात 07:23 से 08:39 तक | उत्तम |
(नोट: उपरोक्त समय दिल्ली के स्थानीय समय के अनुसार हैं और इनमें मामूली क्षेत्रीय भिन्नताएं हो सकती हैं. सटीक समय के लिए स्थानीय पंचांग देखें.)
भाग 2: ब्रह्मांडीय महत्व: दिव्य विश्राम का तत्वज्ञान
देवशयनी एकादशी का महत्व केवल व्रत और मुहूर्त तक सीमित नहीं है. इसका गहरा आध्यात्मिक और पौराणिक आधार है जो हमें ब्रह्मांड की कार्यप्रणाली और देवताओं की भूमिका के बारे में बताता है.
2.1. योगनिद्रा: केवल नींद से कहीं अधिक
जब हम सुनते हैं कि भगवान विष्णु "शयन" करने जा रहे हैं, तो हमें इसे सामान्य नींद नहीं समझना चाहिए. शास्त्रों में इसे योगनिद्रा कहा गया है—एक ऐसी अवस्था जो साधारण, अचेतन निद्रा (तामसिक निद्रा) से बिल्कुल अलग है. योगनिद्रा एक गहरी, सचेत और दिव्य ध्यान की अवस्था है, जिसमें भगवान विश्राम करते हुए भी ब्रह्मांड के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक रहते हैं.
इसका सबसे सुंदर दार्शनिक प्रतीक भगवान विष्णु की वह छवि है जिसमें वे क्षीरसागर में शेषनाग पर लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से निकले कमल पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विराजमान हैं. यह दर्शाता है कि विष्णु की यह "निद्रा" निष्क्रियता नहीं, बल्कि रचनात्मकता का स्रोत है. यह एक ऐसी अवस्था है जहाँ से सृष्टि की संभावनाएँ जन्म लेती हैं. इस प्रकार, चातुर्मास का काल भगवान की अनुपस्थिति का नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय आत्म-चिंतन और ऊर्जा के पुनर्संचय का समय है, जो मानवता को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करता है.
2.2. महान हस्तांतरण: विष्णु से शिव तक
एक और महत्वपूर्ण पौराणिक मान्यता यह है कि जब भगवान विष्णु इन चार महीनों के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं, तो वे सृष्टि के संचालन का कार्यभार भगवान शिव को सौंप देते हैं. यह हस्तांतरण केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है.
भगवान विष्णु का स्वरूप पालन-पोषण और सात्विक ऊर्जा का प्रतीक है, जो सांसारिक गतिविधियों और शुभ कार्यों से जुड़ा है. वहीं, भगवान शिव का स्वरूप तपस्या, वैराग्य और परिवर्तन से जुड़ा है. इसलिए, जब विष्णु विश्राम करते हैं, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा संरक्षण (सत्व) से हटकर तप और आध्यात्मिक शुद्धि की ओर मुड़ जाती है. यह चार महीने का समय ब्रह्मांड के लिए एक तरह का आध्यात्मिक "रीसेट" है, जिसका नेतृत्व संहारक और परिवर्तक, भगवान शिव करते हैं. यह मानवता को भी अपनी बाहरी गतिविधियों को कम करके आंतरिक साधना और तप पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है.
2.3. आस्था को आकार देने वाली कथाएं: मान्धाता और बलि की कहानियां
दो प्रमुख पौराणिक कथाएँ देवशयनी एकादशी के महत्व और इसके व्रत के प्रभाव को स्थापित करती हैं.
राजा मान्धाता की कथा: सतयुग में मान्धाता नामक एक चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजा थे, जो अत्यंत धर्मात्मा और प्रजापालक थे. एक बार उनके राज्य में तीन वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ गया. प्रजा त्राहि-त्राहि करने लगी. अपनी प्रजा के दुख से व्यथित होकर राजा समाधान की खोज में वन में निकल पड़े और अंततः ब्रह्माजी के मानस पुत्र, अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे. अंगिरा ऋषि ने राजा को बताया कि उनके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो उस युग के धर्म के विरुद्ध है, और इसी दोष के कारण वर्षा नहीं हो रही है. ऋषि ने उस शूद्र का वध करने का सुझाव दिया. लेकिन राजा मान्धाता ने एक निरपराध तपस्वी को मारने से इनकार कर दिया और कोई और उपाय पूछा. तब अंगिरा ऋषि ने उन्हें आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी (पद्मा) एकादशी का व्रत अपनी प्रजा सहित करने की सलाह दी. राजा ने विधि-विधान से व्रत का पालन किया, जिसके प्रभाव से राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पुनः सुख-समृद्धि लौट आई. यह कथा इस व्रत की शक्ति को दर्शाती है कि यह न केवल व्यक्तिगत पापों का नाश करता है, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के संकटों को भी दूर कर सकता है.
राजा बलि की कथा: असुर राजा बलि, जो भक्त प्रह्लाद के पौत्र थे, एक महान दानी और पराक्रमी राजा थे. उन्होंने अपने तप और दान के बल पर तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था. इससे भयभीत होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए. विष्णु ने वामन (बौना ब्राह्मण) का अवतार लिया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे. बलि ने वामन को दान मांगने के लिए कहा. वामन अवतार ने उनसे तीन पग भूमि मांगी. बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें चेतावनी दी कि यह स्वयं विष्णु हैं, पर बलि अपने वचन से पीछे नहीं हटे. वामन ने अपने दो पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया. जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया. भगवान विष्णु ने तीसरा पग उनके सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक भेज दिया. बलि की इस महान भक्ति और दानवीरता से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि वे हर साल चार महीने (आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक) उनके साथ पाताल लोक में निवास करेंगे. यही कारण है कि इन चार महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और इस दौरान भगवान विष्णु पृथ्वी पर शुभ कार्यों के लिए उपलब्ध नहीं होते.
भाग 3: भक्ति का मार्ग: व्रत और पूजा की व्यावहारिक मार्गदर्शिका
देवशयनी एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए इसकी पूजा विधि और नियमों का पालन करना आवश्यक है. यह खंड भक्तों के लिए एक विस्तृत, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका प्रदान करता है.
3.1. संपूर्ण पूजन विधि
यह पूजा विधि सुबह से लेकर शाम तक के अनुष्ठानों का विस्तृत विवरण देती है:
- व्रत की तैयारी (दशमी तिथि): व्रत की तैयारी एक दिन पहले, यानी दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाती है. इस रात को सात्विक भोजन करना चाहिए और नमक का सेवन करने से बचना चाहिए.
- प्रातः काल के कृत्य: एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें. पीला रंग भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है.
- संकल्प: हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें. संकल्प मंत्र का उच्चारण करें, जिसमें आप भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे आपको व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति दें.
- पूजा की स्थापना: पूजा स्थल को साफ करके एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं. उस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें. साथ में श्री यंत्र रखना भी शुभ होता है.
- षोडशोपचार पूजन: भगवान का 16 चरणों में पूजन करें. इसमें भगवान को पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण) से स्नान कराना, फिर शुद्ध जल से स्नान कराना, पीले वस्त्र पहनाना, पीला चंदन, पीले फूल, अक्षत और तुलसी दल अर्पित करना शामिल है. ध्यान रहे कि तुलसी दल एकादशी के दिन नहीं तोड़ा जाता, इसलिए इसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें .
- विशेष भोग: भगवान को पीले रंग की मिठाई, जैसे पेड़े, या मौसमी फलों का भोग लगाएं. भोग में तुलसी दल अवश्य शामिल करें, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते.
- शयन की तैयारी (शाम का अनुष्ठान): शाम के समय भगवान विष्णु के शयन की विशेष तैयारी करें. एक छोटे से बिस्तर पर रेशमी या सूती पीले या सफेद वस्त्र बिछाएं. भगवान की प्रतिमा को इस पर लिटाएं. उनके पास तुलसी दल या माला, और धन की स्थिरता के लिए चांदी या पीतल का एक सिक्का पीले कपड़े में लपेटकर रखें.
- शयन मंत्र का जाप: भगवान को शयन कराते समय विशेष शयन मंत्र का जाप करें. यह इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो भक्त को ब्रह्मांडीय घटना से सीधे जोड़ता है.
- आरती और स्तुति: धूप, दीप जलाकर भगवान विष्णु की आरती करें (ॐ जय जगदीश हरे...) और विष्णु सहस्रनाम या अन्य स्तोत्रों का पाठ करें.
- रात्रि जागरण: रात भर जागकर भजन-कीर्तन करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है.
3.2. मंत्रों की शक्ति: दिव्य ऊर्जा का आह्वान
मंत्र ध्वनि की वह शक्ति है जो भक्त को देवता से जोड़ती है. देवशयनी एकादशी पर इन मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होता है:
- शयन मंत्र: सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्तं भवेदिदम्. विबुद्धे त्वयि बुद्धं च जगत्सर्व चराचरम्॥ अर्थ: "हे जगन्नाथ! आपके सो जाने पर यह संपूर्ण जगत सो जाता है. और आपके जागने पर यह संपूर्ण चराचर जगत जागृत हो जाता है." यह मंत्र भक्त के छोटे से अनुष्ठान को ब्रह्मांडीय विश्राम की विशाल घटना से जोड़ता है, यह भाव प्रकट करते हुए कि सृष्टि की चेतना भगवान की चेतना से जुड़ी हुई है.
- भगवान विष्णु का मूल मंत्र: ॐ नमो भगवते वासुदेवाय यह सबसे सरल और शक्तिशाली मंत्रों में से एक है. इसका जाप करने से मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है.
- विष्णु गायत्री मंत्र: ॐ श्री विष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि. तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्॥ यह मंत्र बुद्धि को शुद्ध करने और सही दिशा में मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है.
- नारायण कवच और विष्णु सहस्रनाम: इन स्तोत्रों का पाठ करने से जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं से रक्षा होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है.
3.3. पालन के नियम: क्या करें और क्या न करें
देवशयनी एकादशी से चातुर्मास का आरंभ होता है, इसलिए इस दिन और आने वाले चार महीनों के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है.
तालिका 3: देवशयनी एकादशी और चातुर्मास के नियम
| क्या करें (करणीय) | क्या न करें (वर्जित) | |
| देवशयनी एकादशी के दिन | व्रत: अपनी क्षमता के अनुसार निर्जल, फलाहार या एक समय सात्विक भोजन का व्रत रखें. | नकारात्मक विचार: मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार न लाएं. शांति और सकारात्मकता बनाए रखें |
| पूजा: भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें. तुलसी पूजन का विशेष महत्व है. | तामसिक भोजन: प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन न करें. | |
| दान: अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र या धन का दान करें. | अशुभ कार्य: बाल या नाखून काटना अशुभ माना जाता है. | |
| आचरण: मौन रहें या केवल सत्य और मधुर वाणी बोलें. क्रोध और अहंकार से बचें. | तुलसी तोड़ना: इस दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ें. पूजा के लिए एक दिन पहले ही तोड़ लें. | |
| संपूर्ण चातुर्मास में (4 महीने) | संयम: ब्रह्मचर्य का पालन करें और भूमि पर शयन करें. | मांगलिक कार्य: विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश जैसे कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. |
| सात्विक भोजन: केवल सात्विक भोजन ग्रहण करें. कुछ लोग विशेष वस्तुओं का त्याग करते हैं, जैसे सावन में साग, भादों में दही, आदि. | गलत आचरण: झूठ बोलना, किसी की निंदा करना या किसी को कष्ट पहुंचाने से बचें. | |
| आराधना: नियमित रूप से अपने इष्टदेव की पूजा, मंत्र जाप और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें. | कुछ वस्त्र: नीले और काले रंग के वस्त्र पहनना वर्जित माना जाता है. |
भाग 4: आस्था की नदी: पंढरपुर वारी - एक जीवंत महाकाव्य
देवशयनी एकादशी, जिसे महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है, केवल एक पौराणिक घटना नहीं है. यह पृथ्वी पर भक्ति के सबसे बड़े और जीवंत प्रदर्शनों में से एक का समापन बिंदु है—पंढरपुर वारी. यह एक ऐसी तीर्थयात्रा है जहां लाखों लोग पैदल चलकर अपने प्रिय देवता विट्ठल से मिलने पंढरपुर पहुँचते हैं.
4.1. आषाढ़ी एकादशी: महाराष्ट्र की आत्मा
पंढरपुर वारी 700-800 साल पुरानी एक परंपरा है, जो महाराष्ट्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान का प्रतीक है. यह भक्ति आंदोलन का एक चलता-फिरता, सांस लेता हुआ स्वरूप है, जहां जाति, वर्ग या लिंग का कोई भेद नहीं होता, केवल भक्ति का सागर लहराता है. यह यात्रा आषाढ़ महीने में शुरू होती है और लगभग 21 दिनों तक चलती है, जिसका समापन आषाढ़ी एकादशी के दिन पंढरपुर में होता है.
4.2. वारी के संत: ज्ञानेश्वर और तुकाराम
वारी की आत्मा दो महान संतों—संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम—के दर्शन में निहित है.
- संत ज्ञानेश्वर (13वीं सदी): उन्होंने भगवद्गीता पर 'ज्ञानेश्वरी' नामक टीका लिखी, जिसने अद्वैत वेदांत के गहरे दर्शन को आम लोगों की भाषा मराठी में सुलभ बनाया. उन्होंने ज्ञान और भक्ति के समन्वय पर जोर दिया.
- संत तुकाराम (17वीं सदी): वे एक समाज सुधारक और कवि थे, जिनके 'अभंग' (भक्ति पद) आज भी महाराष्ट्र के घर-घर में गाए जाते हैं. उन्होंने कर्मकांडों पर चोट करते हुए सच्ची, निश्छल भक्ति को सर्वोच्च बताया और सामाजिक समानता का संदेश दिया.
वारी की पूरी यात्रा इन संतों के दर्शन का व्यावहारिक रूप है. पैदल चलना एक तपस्या है, और सामूहिक रूप से अभंगों का गायन ही मुख्य पूजा है. यह ज्ञान और भक्ति को महलों और मठों से निकालकर सड़कों पर ले आती है, जहां हर कोई इसका अधिकारी है.
4.3. पालकी परंपरा: पदचिह्नों की यात्रा
वारी का केंद्र बिंदु 'पालकी' है—एक सजी हुई पालकी जिसमें संतों के प्रतीकात्मक चरण-पादुकाएँ रखी जाती हैं. यह परंपरा 1685 में संत तुकाराम के सबसे छोटे पुत्र, नारायण बाबा ने शुरू की थी. उन्होंने संत तुकाराम की पादुकाओं को पालकी में रखकर यात्रा शुरू की. आज, दो मुख्य पालकियां होती हैं—संत ज्ञानेश्वर की पालकी आलंदी से और संत तुकाराम की पालकी देहू से निकलती है. यह यात्रा संतों के भौतिक शरीर की नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और उनके पदचिह्नों की यात्रा है, जो आज भी लाखों लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं.
4.4. डिंडी: समाज का एक चलता-फिरता मॉडल
लाखों लोगों की यह यात्रा अव्यवस्थित भीड़ नहीं है, बल्कि यह 'डिंडी' नामक इकाइयों में संगठित होती है. एक डिंडी एक ही गांव या समुदाय के वारकरियों (तीर्थयात्रियों) का एक अनुशासित और आत्मनिर्भर समूह होता है. प्रत्येक डिंडी का एक नंबर और जुलूस में एक निश्चित स्थान होता है. डिंडी के प्रबंधक आगे जाकर अगले पड़ाव पर भोजन और आवास की व्यवस्था करते हैं. यह केवल एक यात्रा समूह नहीं है; यह सेवा, समानता और अनुशासन के वारकरी आदर्शों पर बना एक अस्थायी समाज है. यह संगठनात्मक प्रतिभा ही है जो लाखों लोगों को 250 किलोमीटर तक शांतिपूर्वक और व्यवस्थित रूप से यात्रा करने में सक्षम बनाती है.
4.5. वारकरी का अनुभव: आस्था, समानता और तप
वारकरी का अनुभव भक्ति, तप और समुदाय का एक अनूठा मिश्रण है. वे सरल सफेद वस्त्र पहनते हैं, गले में तुलसी की माला और माथे पर चंदन का तिलक लगाते हैं. दिन भर "ज्ञानबा-तुकाराम" के जयकारे लगाते हुए, ढोल और झांझ की ताल पर नाचते-गाते चलते हैं. इस यात्रा में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और सशक्त है. वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, सिर पर तुलसी के पौधे या पानी के बर्तन लेकर यात्रा करती हैं, और भक्ति के इस उत्सव में बराबरी से भाग लेती हैं. यह यात्रा लैंगिक समानता का एक जीवंत उदाहरण है.
4.6. पंढरपुर के स्वामी: विठोबा की अनूठी मूर्ति
पंढरपुर में भगवान विठ्ठल (विठोबा) की मूर्ति अन्य विष्णु रूपों से बिल्कुल अलग है. वे किसी राजसी सिंहासन पर नहीं, बल्कि एक ईंट पर कमर पर हाथ रखे खड़े हैं. यह मुद्रा उनके भक्त पुंडलिक की कथा से जुड़ी है. जब भगवान अपने भक्त पुंडलिक से मिलने आए, तो पुंडलिक अपने माता-पिता की सेवा में इतने तल्लीन थे कि उन्होंने भगवान के खड़े होने के लिए एक ईंट फेंक दी. भगवान ने क्रोधित होने के बजाय, धैर्यपूर्वक उस ईंट पर खड़े होकर अपने भक्त की प्रतीक्षा की. यह मुद्रा भगवान के अपने भक्त के प्रति प्रेम, धैर्य और साक्षी-भाव का प्रतीक है—वे दुनिया के शासक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण द्रष्टा के रूप में खड़े हैं.
4.7. आधुनिक वारी: चुनौतियां और नवाचार
सदियों पुरानी यह परंपरा आज आधुनिक युग की चुनौतियों और नवाचारों का भी सामना कर रही है.
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: वारी अपने मार्ग में आने वाले गाँवों के लिए एक अस्थायी अर्थव्यवस्था का निर्माण करती है. "चलते-फिरते बाज़ार" लगते हैं, जहाँ स्थानीय लोगों को दूध, सब्जियाँ, पूजा सामग्री और अन्य वस्तुएँ बेचकर अस्थायी रोजगार मिलता है.
- पर्यावरणीय प्रभाव: लाखों लोगों के जमावड़े से चंद्रभागा नदी में प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है. स्नान, पूजा सामग्री और अन्य अपशिष्ट नदी के पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव डालते हैं.
- हरित पहल: इस चुनौती का सामना करने के लिए अब कई हरित पहलें शुरू हुई हैं. 'वृक्ष वारी' जैसे अभियानों में स्वयंसेवक यात्रा मार्ग पर हजारों बीज-गेंदे (Seed Balls) फेंकते हैं, ताकि भविष्य के वारकरियों के लिए छायादार पेड़ उग सकें.
- लॉजिस्टिक्स और भीड़ प्रबंधन: सरकार और प्रशासन अब इस विशाल भीड़ के प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं. मोबाइल ऐप के माध्यम से वारकरियों को सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी जाती है, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) की इंसीडेंट रिस्पांस सिस्टम (IRS) जैसी प्रणालियों का उपयोग भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है.
भाग 5: पवित्रता के पीछे का विज्ञान: प्राचीन ज्ञान, आधुनिक सत्यापन
अक्सर आस्था और विज्ञान को दो अलग-अलग ध्रुवों पर देखा जाता है, लेकिन एकादशी व्रत जैसी परंपराओं में प्राचीन ज्ञान और आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का एक अद्भुत संगम दिखाई देता है.
5.1. उपवास का विज्ञान: विषहरण और कोशिकीय मरम्मत
एकादशी का व्रत अनिवार्य रूप से एक प्रकार का आंतरायिक उपवास (Intermittent Fasting) है, जिसके स्वास्थ्य लाभों को आज आधुनिक विज्ञान भी प्रमाणित कर रहा है. जब हम उपवास करते हैं, तो हमारे शरीर को पाचन के निरंतर कार्य से आराम मिलता है. यह ऊर्जा शरीर की मरम्मत और सफाई के कार्यों में लगती है. इस प्रक्रिया को ऑटोफैगी (autophagy) कहा जाता है, जिसमें शरीर अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वयं ही साफ और रीसायकल करता है. यह प्रक्रिया शरीर को विषमुक्त (Detoxify) करने, पाचन में सुधार करने, वजन को नियंत्रित करने और यहाँ तक कि मानसिक स्पष्टता बढ़ाने में भी मदद करती है.
5.2. चावल का रहस्य: यह क्यों वर्जित है?
एकादशी पर चावल न खाने की परंपरा के पीछे पौराणिक और वैज्ञानिक दोनों तरह के कारण बताए जाते हैं.
- पौराणिक दृष्टिकोण: एक कथा के अनुसार, माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने जब अपना शरीर त्यागा, तो उनके अंश पृथ्वी में समा गए और चावल और जौ के रूप में उत्पन्न हुए 76. चूँकि यह घटना एकादशी तिथि को हुई, इसलिए चावल को एक जीव के रूप में देखा जाता है और इस दिन इसका सेवन वर्जित माना जाता है. एक अन्य कथा के अनुसार, ब्रह्मा जी के पसीने से एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने रहने के लिए स्थान मांगा. ब्रह्मा ने उसे एकादशी के दिन मनुष्यों द्वारा खाए जाने वाले चावल के दानों में निवास करने का स्थान दिया.
- वैज्ञानिक दृष्टिकोण: इन कथाओं के पीछे गहरा अवलोकन विज्ञान छिपा हो सकता है. विज्ञान के अनुसार, चंद्रमा पृथ्वी के जल को प्रभावित करता है, जैसा कि ज्वार-भाटा से स्पष्ट है. चावल में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है. माना जाता है कि एकादशी के दिन, जो चंद्र चक्र का ग्यारहवाँ दिन होता है, वायुमंडलीय दबाव सबसे कम होता है. इस समय, यदि अधिक जल तत्व वाली वस्तु (जैसे चावल) का सेवन किया जाए, तो यह शरीर और मन में अस्थिरता पैदा कर सकता है. इससे मन चंचल हो सकता है और व्रत के लिए आवश्यक एकाग्रता बनाए रखना कठिन हो सकता है. आयुर्वेद भी चावल को भारी और 'तमस' (जड़ता) बढ़ाने वाला मानता है, जो आध्यात्मिक साधना के लिए अनुकूल नहीं है. इस प्रकार, एक साधारण नियम, जिसे एक कहानी के माध्यम से पीढ़ियों तक पहुँचाया गया, उसके पीछे चंद्र चक्र और मानव शरीर विज्ञान से जुड़े गहरे वैज्ञानिक सिद्धांत हो सकते हैं.
समग्र संरेखण का एक दिन
देवशयनी एकादशी नियमों और कहानियों का एक बिखरा हुआ संग्रह मात्र नहीं है, बल्कि यह जीवन के लिए एक परिष्कृत और समग्र प्रणाली है. यह हमें सिखाती है कि विश्राम भी एक शक्तिशाली क्रिया हो सकती है, और सच्चा अनुशासन बाहरी आडंबर में नहीं, बल्कि आंतरिक संयम में निहित है.
यह एक ऐसा दुर्लभ दिन है जब ब्रह्मांड (विष्णु का विश्राम, शिव का जागरण), समाज (पंढरपुर वारी का संगम), व्यक्ति (व्रत का संकल्प) और शरीर (उपवास द्वारा शुद्धि) सभी एक साथ एक लय में आ जाते हैं—विश्राम, चिंतन और कायाकल्प की लय में.
इस दिन का संदेश कालातीत है. आज की भागदौड़ भरी, कोलाहलपूर्ण दुनिया में, देवशयनी एकादशी हमें एक आवश्यक ठहराव और आंतरिक शांति का मार्ग प्रदान करती है. यह एक अनुस्मारक है कि कभी-कभी, सबसे बड़ी प्रगति बाहरी दुनिया में दौड़ने से नहीं, बल्कि भीतर की ओर मुड़ने से होती है.








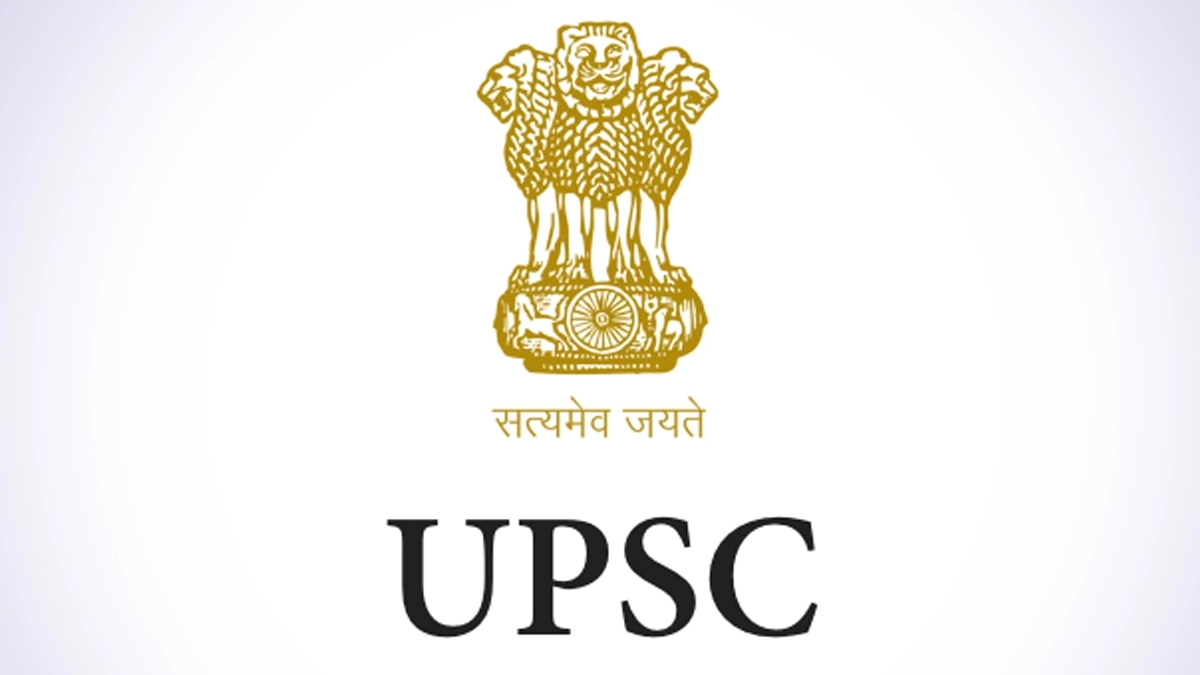

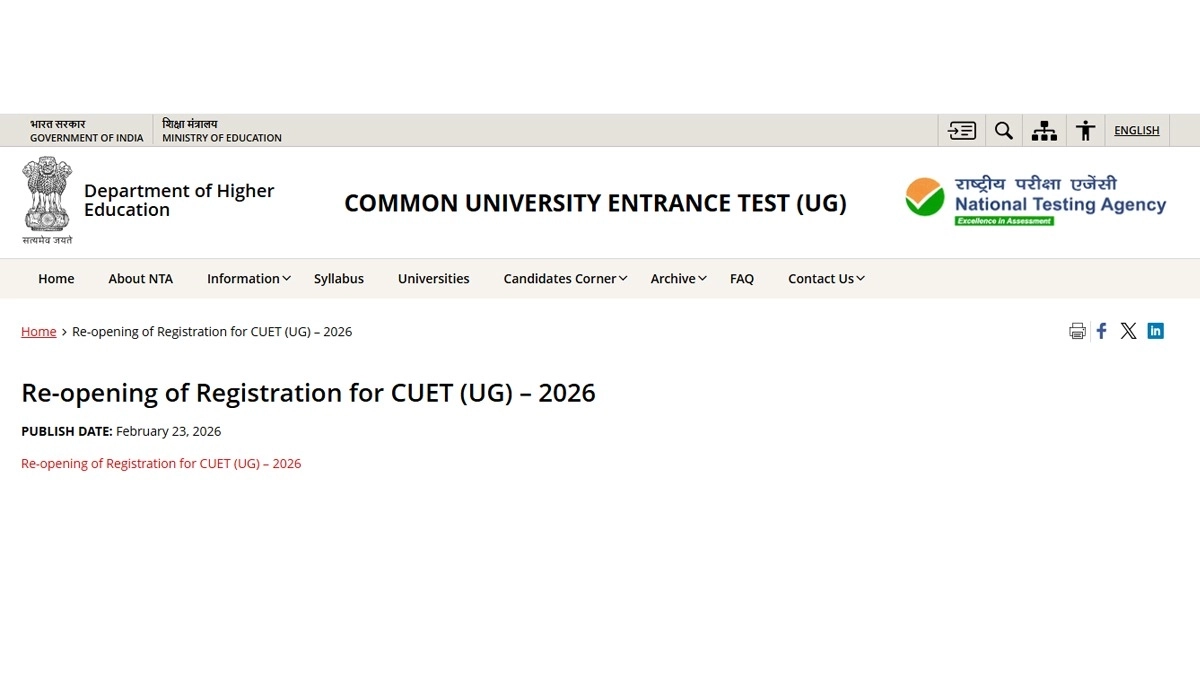
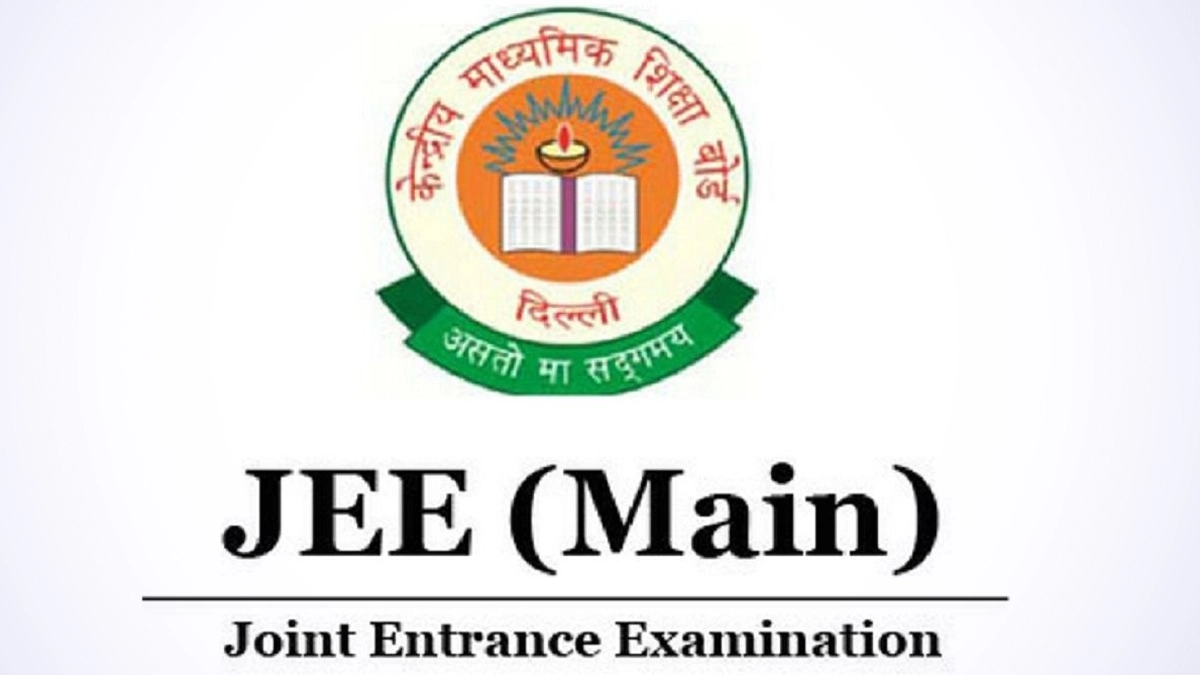

 QuickLY
QuickLY