
अमेरिका ने आईसीसी पर प्रतिबंध लगा दिए हैं. वह डब्ल्यूएचओ से भी बाहर निकल गया है. वैश्विक संस्थानों के सामने वजूद का संकट खड़ा हो गया है.अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत (आईसीसी) से इस्राएली प्रधानमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के जवाब में आईसीसी पर प्रतिबंध लगाने के कार्यकारी आदेश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने हस्ताक्षर कर दिए हैं. इन प्रतिबंधों में वित्तीय प्रतिबंध और आईसीसी अधिकारियों के वीजा रद्द करना शामिल हैं. आईसीसी ने बीते साल नवंबर में बेन्यामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योआव गालांत के खिलाफ वारंट निकाला था.
दुनिया में संरक्षणवाद, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक खतरों के बढ़ने के साथ ही, अंतरराष्ट्रीय नियामक संगठनों के अस्तित्व पर संकट नजर आने लगा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन और पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने जैसी घटनाएं वैश्विक सहयोग के लिए एक बड़ी चिंता बन गई हैं.
नया नहीं है संकट
ऐसा नहीं है कि यह कोई पहली बार हो रहा है. 1930 के दशक में भी इन संगठनों के लिए ऐसा ही समय आया था, जब वैश्वीकरण में गिरावट और संरक्षणवाद का उभार हुआ था.
2021 में आई एक रिपोर्ट में लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर पेरी 6 और मार्थ प्रेवेजेर ने यॉर्क यूनिवर्सिटी की एवा हीम्स के साथ मिलकर एक अध्ययन किया था. उन्होंने इस बात को अच्छे से समझाया था कि ये अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं 1930 के दशक में किस तरह चुनौतियों के सामने टिके रहे थे.
यह ऐतिहासिक उदाहरण संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक संस्थानों जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए महत्वपूर्ण है. रिपोर्ट में लेखक कहते हैं कि जब किसी संगठन का प्रभाव कम हो जाता है, तब अगर वह बुनियादी और आवश्यक कार्यों को संभालता है, तो वह प्रभावी रूप से कार्य करना जारी रख सकता है. मसलन, डब्ल्यूएचओ को अमेरिका के बाहर निकलने से बड़ा धक्का लगा है, तब भी वैश्विक स्वास्थ्य ढांचे में उसकी भूमिका का कोई और विकल्प दुनिया के पास नहीं है. यह कुछ वैसा ही है, जैसे 1930 के दशक में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) का था.
इस रिपोर्ट में दुनिया के तत्कालीन संगठनों के उदाहरण देकर पेरी और उनके साथियों ने दिखाया कैसे उन्होंने संकटों का सामना और उनके हिसाब से खुद को तैयार किया. वे लिखते हैं, "1931 में वैश्विक आर्थिक संकट के बाद इन संगठनों ने विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाने में असमर्थता महसूस की. तब उन्होंने अपना ध्यान मौजूदा नियमों और सूचना सेवाओं के प्रबंधन पर लगाया."
रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) और आर्थिक और वित्तीय संगठन (ईएफओ) का अध्ययन कर तैयार की गई है, जो 1930 के दशक में श्रमिक संबंधों और वित्तीय निगरानी के लिए जिम्मेदार थे. ये समूह अधिक तेजी से बदलने वाले क्षेत्र थे. रिपोर्ट के लेखक बताते हैं कि वैसे समय में वैश्विक प्रभाव वाले नेताओं ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर इन संगठनों का वजूद बचाया था.
उदाहरण के लिए तब आईएलओ सामाजिक बीमा योजनाओं के डिजाइन पर दक्षिण अमेरिकी सरकारों को तकनीकी सहायता प्रदान करने में सफल रहा और ईएफओ ने संकटग्रस्त देशों जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ वित्तीय समझौतों पर बातचीत की. 1941 से 1948 के बीच आईएलओ के महानिदेशक रहे एडवर्ड फीलन जैसे प्रभावशाली नेता अपने नेटवर्क और प्रभाव का उपयोग कर पाए इस संगठन को बचा पाए. इसी तरह के प्रयासों ने दूसरे संगठनों को भी बचाया.
इन संगठनों का अस्तित्व वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद बना रहा, और यहां तक कि 1970 के दशक तक जारी रहा. आज डब्ल्यूटीओ जैसी वैश्विक व्यापार संस्थाओं का अस्तित्व इस बात पर निर्भर कर सकता है कि वे शक्तिशाली देशों के बीच सहयोग को कैसे बढ़ावा देती हैं, भले ही वे संरक्षणवाद का सामना कर रहे हों.
21वीं सदी में वैश्विक सहयोग
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और कंसल्टेंसी फर्म मैकिंजी ने ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर रिपोर्ट में कहा है कि दुनिया के बीच सहयोग इस वक्त बेहद गंभीर संकट से गुजर रहा है. 2025 का बैरोमीटर दिखाता है जबकि वैश्विक सहयोग महामारी से पहले के स्तर से अधिक है, पिछले तीन वर्षों में यह आगे नहीं बढ़ पाया है. इसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा में गिरावट, और व्यापार और पूंजी सहयोग में कमी को प्रमुख कारण बताया गया है. हालांकि, जलवायु और प्राकृतिक पूंजी के क्षेत्र में सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं, जहां यूएन का पैक्ट ऑफ द फ्यूचर 2024 में अपनाया गया था.
पेरी, हीम्स और प्रेवेजर का ऐतिहासिक विश्लेषण इस बात का संकेत देता है कि वैश्विक संस्थानों को अस्तित्व में बने रहने के लिए नई रणनीतियां अपनानी पड़ेंगी. वे कहते हैं, "कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी, यह दो बातों पर निर्भर करता है. पहला, उस क्षेत्र की विशेषताएं जो नियमित की जा रही हैं. और दूसरा, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और सदस्य देशों के भीतर अनौपचारिक सामाजिक संगठन.” इसका मतलब है कि संगठनों को बदलती वैश्विक गतिशीलता के साथ तालमेल बिठाते हुए मजबूत और लचीले नेटवर्क और नेतृत्व को बढ़ावा देना होगा.
आगे का रास्ता: प्रतिस्पर्धा के बीच सहयोग
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि आज के नेताओं के सामने एक विभाजित भू-राजनीतिक परिदृश्य में प्रतिस्पर्धा और सहयोग के बीच संतुलन बनाए रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. ग्लोबल कोऑपरेशन बैरोमीटर में यह सुझाव दिया गया है कि वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नेताओं को पहले वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना होगा और फिर सहयोग के नए तरीकों के प्रति खुले दिमाग से सोचना होगा. उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि "सरकारें नए संवाद स्थापित करें और संचार के नए रास्ते खोलें.” मसलन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन संस्थानों के जरिए वैश्विक सहयोग को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की थी.
अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को विकसित होने की आवश्यकता होगी. चाहे वे मौजूदा कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें, नेतृत्व को सशक्त बनाएं या अनौपचारिक नेटवर्क का लाभ उठाएं. पेरी, हीम्स और प्रेवेजर कहते हैं कि जब वैश्वीकरण फिर से मजबूत होगा तो कुछ संगठनों को अपनी क्षमता नई एजेंसियों को सौंपनी पड़ सकती है या नए अंतरराष्ट्रीय संस्थान उभर सकते हैं जो बदलते उद्योगों और परिस्थितियों का जवाब देंगे.


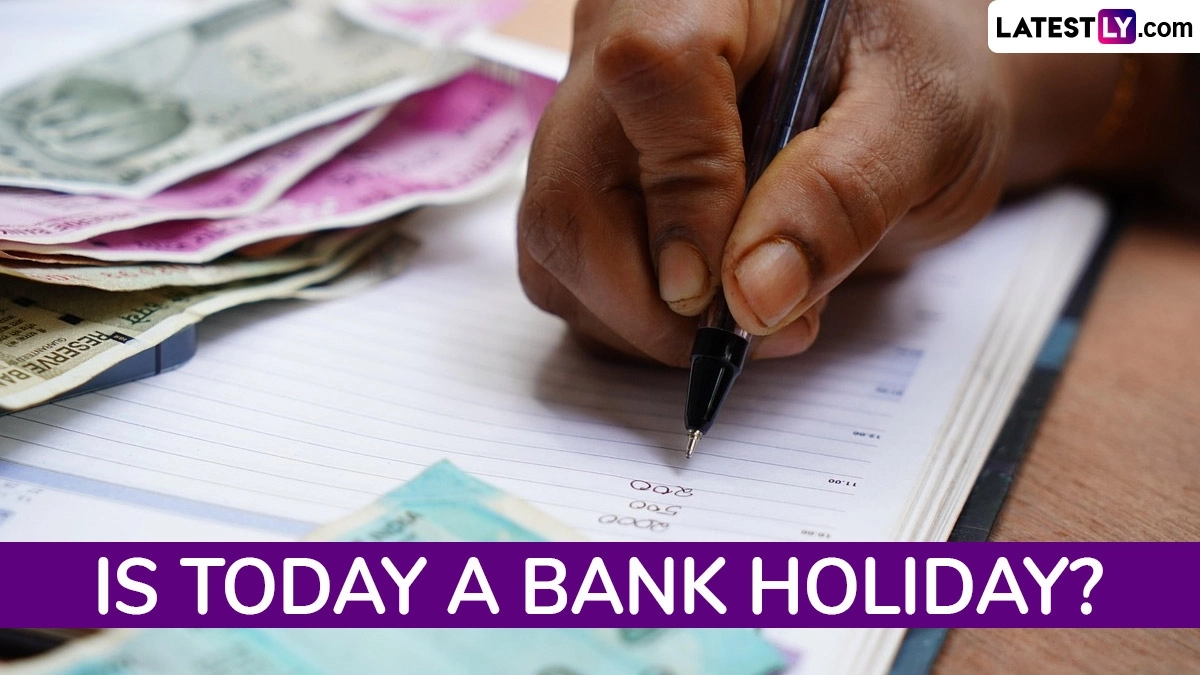










 QuickLY
QuickLY